नदी जोड़ परियोजना : विकास या विनाश
पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल से भरा है मगर पीने के लिए मीठा पानी बहुत कम है। कुल उपलब्ध पानी का मात्र 3 फ़ीसदी मीठा पानी है । दुनिया के 100 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। 270 करोड लोगों को साल में एक महीना पीने का पानी नहीं मिलता । संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार 2030 तक वैश्विक स्तर पर पीने के पानी की मांग आपूर्ति से 40 फ़ीसदी अधिक हो जाएगी । एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 11 बड़े शहर बूंद बूंद पानी के लिए तरससेंगे, इनमें केपटाउन ,लंदन ,मास्को, बीजिंग, टोक्यो आदि बड़े शहर शामिल है।
भारत में भी जल संकट गहराता जा रहा है। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी हो रही है ।आजादी के समय जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति सालाना 3400 घन मीटर था । लेकिन अब घटकर 1000 घन मीटर रह गया है । जाहिर है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में तेजी से कमी हो रही है ।संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्धता से कम पानी वाला देश जल संकट की श्रेणी में आता है । गंभीर जल का सामना कर रहे दुनिया के प्रमुख 11 शहरों में भारत का बेंगलुरु शहर भी है। बेंगलुरू शहर के झीलों का 85 फीसदी पानी केवल सिंचाई या फैक्टरी के इस्तमाल लायक है।
देश में एक तरफ जहां केरल राज्य बाढ़ का दंश झेल रहा है वहीं बिहार में सूखे की स्थिति है । धरती के तापमान में हो रहे बढ़ोतरी के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है । परिणाम स्वरूप बारिश अनियमित हो रही है या बेहद कम। मानसून के 3 महीने में मुश्किल से 40 दिन पानी बरसता है या फिर 1 सप्ताह में ही लगातार बारिश हो जाना या बहुत कम बरसना यह सभी परिस्थितियां नदियों के लिए अस्तित्व का संकट केंद्र पैदा कर रही है।
केंद्र सरकार जल के गहराते संकट के समाधान के लिए नदी जोड़ परियोजना ला रही है। नदी जोड़ परियोजना में 30 लिंक बनने हैं। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दी है। पहला नदी जोड़ परियोजना केन बेतवा लिंक को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। 18000 करोड़ की लागत से बनने वाली केन बेतवा लिंक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से शामिल हैं। मध्य प्रदेश के केन के अतिरिक्त पानी 231 किलोमीटर लंबी शहर के जरिए उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में लाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड की 6.35 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर , पन्ना, टीकमगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा एवं महोबा जिले के लोग इससे लाभान्वित होंगे। सरकार का मानना है कि नदी जोड़ परियोजना में कुल 30 लिंक बनने के बाद 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दावा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात मिलेगी क्योंकि अतिरिक्त जल के इस्तमाल की व्यवस्था मौजूद रहेगी।
केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना के दो घटक हैं– हिमालय नदी विकास एवं प्रायद्वीपीय नदी विकास। हिमालय नदी विकास में भारत, नेपाल एवं भूटान में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों का भंडारण , जलाशयों का निर्माण करने तथा गंगा के पूर्वी सहायक नदियों के प्रवाह को पश्चिम में स्थानांतरित करने के उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ने और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों को गंगा से तथा गंगा को महानदी से जोड़ने पर जोर दिया गया है।
प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। महानदी, गोदावरी , कृष्णा एवं कावेरी को आपस में जोड़ना तथा इसके बेसिन में जलाशयों का निर्माण करना।
मुंबई के उत्तर में तथा तापी के दक्षिण में पश्चिममीवर्ती प्रवाही नदियों को आपस में जोड़ना केन एवं चंबल को आपस में जोड़ना तथा पश्चिमीवर्ती प्रवाही नदियों का जल नहर के जरिए अन्यत्र ले जाना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नदी घाटी के निकट भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जल को कमी वाले नदी घाटी क्षेत्र में ले जाना है । जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार तीन संपर्कों नामतः केन बेतवा संपर्क, दमन गंगा, पिंजाल संपर्क और पर, तापी ,नर्मदा संपर्क पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है।
देश के 12% हिस्सा बाढ़ एवं 68% हिस्सा सूखे से प्रभावित रहता है । सरकार का मानना है कि नदी जोड़ परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद देश को बाढ़ एवं सूखा की समस्या से निजात मिल जाएगी । राष्ट्रीय परिपेक्ष के अनुसार ( आधार वर्ष 2002 ) के अनुसार देश में नदियों को जोड़ने का अनुमानित लागत 5, 60,000 करोड़ रुपया होगा । इसके तहत 30 संपर्कों के लिए लगभग 3000 छोटे – बड़े जलाशयों का निर्माण होगा। लगभग 12.5 हजार किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण होगा। संपूर्ण परियोजना को पूरा होने में 30 – 35 साल लगेगा।
वैसे नदी जोड़ परियोजना का इतिहास बहुत पुराना है। भारत की सारी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव सबसे पहले ब्रिटिश राज में चर्चित इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने 1858 में दिया था । उनकी सोच यह थी कि नहरों के विशाल जाल के जरिए नदियां आपस में जुड़ जाएंगी। इससे ब्रिटिश साम्राज्य के इस उपनिवेश में आयात निर्यात का काम सुगम हो जाएगा । सूखे एवं बाढ़ की समस्या से भी निपटारा होगा। लेकिन तब संसाधनों के अभाव में यह परियोजना आगे नहीं बढी। आजादी के बाद 1970 में नदी जोड़ परियोजना फिर सुर्खियों में आई , जब तत्कालीन सिंचाई मंत्री के एल राव ने एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने का प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी घाटी में ज्यादा पानी रहता है जबकि मध्य और दक्षिण भारत में पानी की कमी है। इसके तहत (गंगा कावेरी ) ढाई हजार किलोमीटर नहर द्वारा गंगा के करीब 50000 क्यूसेक पानी लगभग 500 मीटर ऊंचा उठाकर दक्षिण भारत की तरफ लाया जाना था। केंद्रीय जल आयोग ने इस परियोजना को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बता कर खारिज कर दिया।
फिर नदी जोड़ परियोजना की चर्चा 1980 में हुई । इस साल जल संसाधन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की थी नेशनल पर्सपेक्टिव आफ वॉटर डेवलपमेंट । नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने 1982 एक रिपोर्ट तैयार की मगर बात आगे नहीं बढ़ी । 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। जिसने अपनी रिपोर्ट में परियोजना को दो भागों में बांटने की सिफारिश की। पहले हिस्से में दक्षिण की 16 नदियों को जोड़ कर दक्षिण में 1 ग्रिड बनाया जाए। हिमालयी हिस्से के तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को जोड़ने की योजना बनाई । 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद मामला फिर खटाई में पड़ गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे समयबद्ध तरीके से अमल करें । अब केन बेतवा लिंक के साथ नदी जोड़ परियोजना जमीन पर उतरने वाली है।
लेकिन तमाम तर्को, दावों एवं आश्वासनों के बीच नदी जोड़ परियोजना के बारे में लोगों के मन में आशंका के बादल मंडराने लगे है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर करना निहायत जरूरी है । पर्यावरणविद् मानते हैं कि इतने व्यापक पैमाने पर प्रकृति के साथ छेड़ – छाड़ के नतीजे भयानक होंगे ।हम मुंबई ,चेन्नई ,उत्तराखंड में केदार घाटी त्रासदी और अभी हाल में केरल में आए महा विनाशकारी बाढ़ से सबक सीखने के बजाय उसे दोहराने में लगे हैं । नदियों के भूगर्भीय स्थिति ,उसमें गाद आने की मात्रा, देश में दूसरी परियोजनाओं के अनुभव एवं विदेशों में ऐसी परियोजनाओं के हश्र पर गौर करने से स्पष्ट हो जाता है कि नदी जोड़ परियोजना के परिणाम विनाशकारी सिद्ध होंगे।
पर्यावरण एवं नदी मामलों के विशेषज्ञ अनुपम मिश्र का मानना था कि नदी कोई रेलगाड़ी नहीं जिसे दो पटरियों के बीच चलाया जाए ।नदियों का अपना एक स्वाभाविक ढाल होता है, जिसे वह अपने आप पकड़ती है ।आसपास के इलाकों को खुशहाल बनाते हुए आगे बढ़ती है । ऐसे कई उदाहरण हैं जब नदियों के पानी की दिशा नहरों द्वारा बदली गई तो आसपास का इलाका खारा और दलदली बना । उत्तर प्रदेश के 16 जिलों से गुजरने वाली शारदा सहायक नहर जो देश के प्रमुख नहरों में से एक है सन 2000 में पूरी हुई। 1260 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का लक्ष्य 16.77 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना था । लेकिन लक्ष्य का सिर्फ 48% ही हासिल हो पाई । इससे रिसता पानी हजारों हेक्टेयर भूमि में जल जमाव एवं सीलन के कारण बन रहे हैं। इससे कम पानी की फसलें गेहूँ, तेलहन आदि बर्बाद हो रहे हैं।
शारदा सहायक नहर में तेजी से भरने वाला गाद नहर के पानी ले जाने की क्षमता को कम कर रही है। इसके साथ ही खेती की जमीन को बंजर बना रही है। नहर के बारे में बढ़ रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने नहर से गाद निकालने के लिए 319 करोड़ का विशेष पैकेज दिया था । उल्लेखनीय है कि यह नहर रायबरेली होकर भी जाती है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृ एवं पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है।
राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा कई दशकों से अदालती पेंच में फंसा है। 1981 में पंजाब , हरियाणा , दिल्ली एवं राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत पंजाब को सतलज का पानी अन्य राज्यों को बांटना था। लेकिन बाद में पंजाब इस वादे से मुकर गया । उसका कहना है कि सतलज सिर्फ पंजाब में बहती है । इसका पानी वह अन्य राज्यों को क्यों बांटे । इस मुद्दे पर राज्य के सभी दलों में एकता है । इसी प्रकार कावेरी जल को लेकर विवाद बहुत पुराना है। नदी जोड़ परियोजना में 30 नदियों को जोड़ना है। ऐसे में इसका नतीजा क्या होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।
बात सिर्फ राज्यों के बीच होने वाले विवाद का नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय मामला भी बनेगा । भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था , जिसके अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा के निकट फरक्का बराज से पहले किसी भी इलाके में गंगा के पानी को किसी दिशा में नहीं मोड़ेगा। नदी जोड़ परियोजना से गंगा के पानी को लेकर भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ेगा।
विडंबना है कि जब विदेशों में इस प्रकार की परियोजनाओं के दुष्परिणाम आने के बाद इसे बंद किया जा रहा है तब भारत में इसे विकास के नाम पर लाया जा रहा है । अमेरिका में कोलोराडो से लेकर मिसीसिपी नदी घाटी तक बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं में गाद भरने के बाद बाढ़ का प्रकोप बढ़ने लगी । बिजली का उत्पादन भी धीरे-धीरे घटने लगा । आखिर में इस परियोजना में बने बांध को तोड़ने पड़े । इस पर जो खर्च हुआ वह अलग । स्मरण है बड़े बांधों को तोड़ने का काम भी काफी खर्चीला है । गंगा , ब्रह्मपुत्र में आने वाली गाद मिसीसिपी नदी से दोगुना है । ऐसी परिस्थिति में नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र आदि हिमालयी नदियों पर बनने वाले बांधों का भविष्य क्या होगा इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। साइबेरियाई नदियों को नहरों के जाल के माध्यम से काजिस्तान और मध्य एशिया के कम पानी वाले नदियों की ओर मोड़ने का काम हुआ। जहां जहां नहर पहुंची वहां वहां दलदली एवं खारे पानी ने किसानों की कमर तोड़ दी । अंत में 80 के दशक में इस परियोजना को छोड़ देना पड़ा।
सवाल उठता है कि समाधान क्या है? भारत में जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था रही है । जल प्रबंधन के छोटे-छोटे स्थानीय प्रयासों से कम बारिश वाले इलाकों में भी नदियों को पुनर्जीवित करने के सफल उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे इलाके के नदियों के पानी को खींचकर ले जाने की जटिल और विनाशकारी काम की क्या आवश्यकता है ? जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा और बड़े पैमाने पर भौगोलिक बिगाड़ भी होगा । गंगा मुक्ति आंदोलन के नेता अनिल प्रकाश कहते हैं कि इस परियोजना से लाभ की तुलना में हानि ज्यादा होगा। इसमें जंगलों का विनाश होगा और जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और खराब होगी।
पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र का मानना था की नदी जोड़ने का काम प्राकृतिक करती है। जहां दो नदियां जुड़ती है वह तीर्थ स्थल बन जाता है। जब दो नदियों को नहरों से जोड़ने की कोशिश होती है तो किसान को तो नहीं नेताओं और बाबूओं को लाभ होता है। देश में पानी की समस्या का सही हल सही जल प्रबंधन है । जितना पैसा नदियों को जोड़ने पर खर्च होगा उससे कहीं कम में नदियों और तालाबों को बचाने और बारिश के पानी रोकने से समस्या हल हो जाएगी। देश में पानी सहजना एवं जल प्रबंधन के कम लागत वाले तरीके मौजूद है। लेकिन सरकार इसे अपनाना नहीं चाहती ।यह जल संकट का मुख्य कारण है ।
विकास के उसी मॉडल का भविष्य है जिसमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की तैयारी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने का सामर्थ है मगर एक भी व्यक्ति की लालच पूरा करने का सामर्थ नहीं है। विकास के भोगवादी मॉडल के कारण ही यह संकट उत्पन्न हुआ है । हमें अपने सोच में रचनात्मक बदलाव लाना होगा वरना इस सभ्यता का कोई भविष्य नहीं है।
अशोक भारत
मो. 9430918152
Email- bharatashok@gmail.com

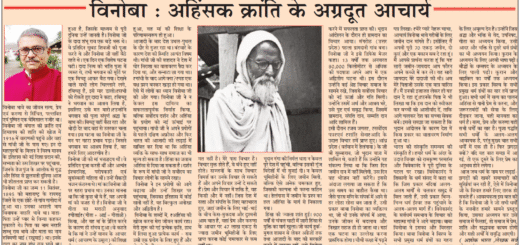

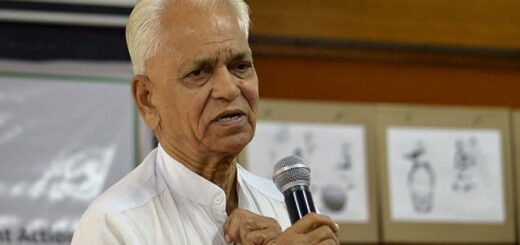
Recent Comments