प्रेमचंद : नई सभ्यता के स्वप्नदर्शी
कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उन विरले लेखकों में हैं जिनकी रचनाएं उनकी मृत्यु के आठ दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सबसे ज्यादा पसंद और पढ़ी जाती है । प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में किसान, मजदूर, हिंदू – मुस्लिम एकता, जाति, स्वराज, सामंतवाद , उपनिवेशवाद और महाजनी सभ्यता के सवाल को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने तीन सौ से ज्यादा कहानियां, लगभग एक दर्जन उपन्यास के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं जिसमें उनके लेखकीय कौशल और विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है, जो आज भी असंख्य पाठकों को प्रभावित और प्रेरित करता है। प्रेमचंद ने पहला उपन्यास ‘सेवासदन’ सन् 1918 में लिखा और अंतिम उपन्यास ‘गोदान’ सन् 1936 में। यह काल हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के बाद यह काल हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्व का माना जाता है । जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रुढियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। प्रसिद्ध आलोचक डा. नामवर सिंह का कहना है कि ‘छायावाद वस्तुतः एक व्यापक जीवन दृष्टि थी जिसकी अभिव्यक्ति सामान्य रूप से कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि सभी माध्यमों में हुई परंतु भावनात्मकता के कारण उसकी विशेष अभिव्यक्ति कविता में ही हो सकी और उसी से उसे प्रधानता भी मिली। ( छायावाद और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां) ‘प्रेमचंद की वैचारिक संवेदना’ के लेखक और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. योगेन्द्र का कहना है कि ‘प्रेमचंद का कालखण्ड छायावाद का कालखंड है। सभी आलोचकों ने इस काल की कविताओं को सर्वप्रमुख विशेषता – ‘व्ययक्तिकता’ बतायी है। प्रेमचंद ने व्ययक्तिकता को तरजीह नहीं दी। उनका विश्वास सामाजिकता में था।’
प्रेमचंद की रचनाओं में जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किसानों और मजदूरों के शोषण को प्रमुखता से जगह मिली है। उनके उपन्यास और कहानियों में इसका बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण देखने को मिलता है। यह प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषता है। प्रेमचंद सामंतवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। छायावाद काल खंड में वे कलम के मजदूर तो थे ही इसके साथ साथ वे सामंती और उपनिवेशवाद की प्रवृत्तियों के खिलाफ एक योद्धा भी थे। प्रेमचंद्र ने जातिवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। वह हिंदू मुस्लिम एकता को स्वराज के लिए आवश्यक मानते थे और सांप्रदायिकता के सख्त खिलाफ थे। वे स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और मानते थे कि हर एक विषय में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए । इसलिए उनकी स्वराज की कहानियों में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में है। चाहे जुलूस की मिट्ठनबाई हो या पत्नी से पति की गोदावरी वह अपने पति से विद्रोह करती है, जो सरकारी सेवक है और खुद स्वराज आंदोलन में शरीक होती है । अंत में अपने पति का हृदय परिवर्तन कराने में सफल होती है। समर यात्रा की नोहरी अदम्य साहस और देश भक्ति की बेमिसाल नजीर है। बुढापे में भी वह न केवल सत्याग्रहियों की जत्था का स्वागत करने और उसमें शामिल होने के लिए गांव के लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है, बल्कि पुलिस की भी निर्भीकता से मुकाबला करती है। और अंत में सत्याग्रहियों की टोली में शरीक हो जाती है।
प्रेमचंद्र सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे । वे धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर करते थे । लेकिन वे धर्म को कोई गैर जरूरी चीज नहीं मानते थे। उनकी लेखनी में गांधी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। गांधीजी धार्मिक व्यक्ति थे। वे खुद को सनातनी हिंदू मानते थे । मगर वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। अप्रैल 1931 में कांग्रेस का एक सम्मेलन मिर्जापुर में हुआ था जिसमें युसूफ इमाम ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस वाले को सांप्रदायिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रेमचंद ने इसकी प्रशंसा की थी । धर्म और सांप्रदायिकता के बारे में उनकी बिल्कुल साफ समझ थी। वे कहते हैं कि ‘जो मनुष्य धर्म शून्य है , वह राष्ट्रीयता के भाव से भी शून्य होगा । धर्म ईश्वर और मनुष्य के संबंध की वस्तु है । धर्म इतना उदार होना चाहिए कि यदि हमारा पुत्र या स्त्री किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हो जाए तो जरा भी शोक या ताप न हो ।’ (विभिन्न प्रसंग भाग -2 पृष्ठ सं. 266 ) प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और इसे मजबूत करना चाहते । 1932- 34 के बीच हिंदू मुस्लिम एकता पर छ: महत्वपूर्ण लेख लिखें। उन्होंने उनकी प्रशंसा की जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे और उन सब की आलोचना की जो साम्प्रदायिकता के प्रत्यक्ष या परोक्ष पक्षधर थे। कानपुर दंगा रिपोर्ट के लिए डा. भगवान दास और पंडित सुंदरलाल की दिल खोलकर प्रशंसा की । आचार्य चतुरसेन शास्त्री की ‘इस्लाम का विषवृक्ष’ पुस्तकों के लिए कठोर आलोचना की। देश समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बेमिसाल थी। उनकी सांप्रदायिकता संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक है।
प्रेमचंद की कहानियां में स्वराज आन्दोलन का प्रभाव देखने को मिलता है। जुलूस, जेल, समर यात्रा, पत्नी से पति , दुनिया का सबसे अनमोल रतन आदि अनेक स्वराज की कहानियां उन्होंने लिखी। प्रेमचंद जनता की जागृति को स्वराज के लिए आवश्यक मानते थे। प्रेमचंद ने 1907 में अपनी पहली कहानी ‘दुनिया का सबसे अनमोल रतन’ में लिखा कि ‘ खून की वह आखरी बूंद जो देश की आजादी के लिए गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है’ उनका दृढ़ विश्वास था हिंदुस्तान का उद्धार हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार यह भाव पैदा करना प्रत्येक देशवासी का परम धर्म है। यही कारण है कि जब आलोचक असहयोग आंदोलन की आलोचना कर रहे थे प्रेमचंद इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे । वे लिखते हैं कि ‘हम यह दावा करना अपने तई ठीक समझते हैं कि स्वराज का आंदोलन अब तक कामयाब हुआ है। विद्यार्थियों ने सामूहिक रुप से कॉलेज – स्कूल न छोड़े हो, लेकिन उनमें आजादी और सच्चाई की चेतना, सेवा और बलिदान की भावना जरुर पैदा हो गई है जो आगे चलकर राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होगी।’ (विभिन्न प्रसंग भाग 2 पृष्ठ 22) प्रेमचंद जनता की जागृति को स्वराज के लिए आवश्यक मानते थे तथा जमींदार और पूंजीपति को इस रास्ते के रोड़े। इसके साथ हिंदू – मुस्लिम, छुआछूत के मसले भी स्वराज के लिए वे बाधा मानते थे। वे कहते हैं कि ‘हमारे समाज में अभी ऊंच-नीच का विचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। चमार अभी भी अछूत है और डोम का स्पर्श करना हमारे लिए घोर पातक है। मनुष्य की आत्मा की श्रेष्ठता उसका गौरव हम भूल बैठे हैं।(वि.प्र.पृ 21) ‘ अपनी कल्पना के स्वराज के बारे में वे लिखते हैं कि ‘अपने देश का पूरा का पूरा इंतजाम जब जनता के हाथों में हो तो उसे स्वराज कहते हैं। जिन देशों में स्वराज है वहां प्रजा अपनी ही चुने हुए पंचों द्वारा अपने ऊपर राज करती है। वहां यह नहीं हो सकता की प्रजा लगान और कर के बीच में दबी रहे और अधिकारी लोग दिनोंदिन सेना बढ़ाते जाएं, कर्मचारियों का वेतन बढाते जाएं। अधिकारी लोग प्रजा पर उनके हितों के लिए नहीं , बल्कि अपने प्रभुत्व जमाने और भोग विलास के लिए राज करते हो।’ ( विविध प्रसंग भाग -2, पृ 271) वे लिखते हैं कि ‘स्वराज मिलने से देश में सुख और शांति का स्वराज हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे कैदी जेल से छूटकर सुखी होता है। स्वराज हमारी बुद्धि को, हमारी विचार – शक्ति को मुक्त कर देगा और संसार में फिर उसकी आवाज सुनाई देगी। हम संसार को एक नई सभ्यता, एक नए जीवन का प्रचार कर देंगे। स्पर्धा और प्रतिद्वंदिता को मिटाकर सहकारिता और प्रेम का सिक्का जमा देंगे।’ बिडम्बना देखिए प्रेमचंद ने जो गुलाम भारत में देखा, लिखा कमोबेश आज आजाद भारत में भी वही सब घटित हो रहा है। कहने के लिए हम लोकतांत्रिक देश हैं। मगर आज लोक पर तंत्र ही हावी है। भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों ,धनपशुओं और बाहुबलियों ने इसका अपहरण कर लिया है। आचार्य जानकीबल्लभ शास्त्री की ये पंक्तियां आज की व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठती हैै
‘कुपथ कुपथ में रथ दौड़ता जो , पथ निर्देशक वह है,
लाज लजाती है जिनकी कृति से, धृति उपदेशक वह है ‘
प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में किसानों और मजदूरों के सवाल को प्रमुखता से उठाया । उनकी रचनाओं में किसानों की पीड़ा, शोषण, दुर्दशा का सजीव चित्रण देखने को मिलता है । चाहे ‘पूस की रात ‘ हो या ‘सवा सेर गेहूं’ या’ हतभागे किसान’ या अन्य कोई रचनाएं, इन सब में उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक चित्र प्रस्तुत किया है। 19 दिसंबर 1932 को हंस में प्रेमचंद ने एक लेख लिखा ‘हतभागे किसान ।’ इसमें वे लिखते हैं ‘भारत के 80 फीसदी आदमी खेती करते हैं। कई फीसदी वे हैं जो अपनी जीविका के लिए किसानों के मोहताज है जैसे गांव में बढ़ाई, लोहार आदि । राष्ट्र के हाथ में जो कोई विभूति है वह इन्हीं किसानों के मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और विद्यालय , हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें और कचहरियां सब इन्हीं की कमाई के बल पर चलती हैं। लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न वस्त्र दाता हैं भरपेट अन्न को तरसते हैं, जाड़े पाले में ठिठुरते हैं और मक्खियों की तरह मर जाते हैं।’ आज आजादी के 73 साल बाद भी किसानों की स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। वे लिखते हैं कि ‘किसानों को संरक्षण की इसलिए जरूरत है कि वे दीन और अशक्त हैं। एक ओर जमींदार के शिकार हो रहे हैं तो दूसरी और साहूकार के। आज जमींदार की जगह बाजार ने ले ली हैंऔर सरकारें बाजार की मददगार ।
1936 में प्रेमचंद्र ने अपनी चर्चित लेख ‘महाजनी सभ्यता’ लिखी। ‘महाजनी सभ्यता’ युग का दस्तावेज है । वे लिखते हैं कि ‘इस महाजनी सभ्यता के सारे कामों की गरज पैसा होती है। किसी देश पर राज किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों, पूंजीपतियों का ज्यादा से ज्यादा नफा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का राज है । अधिक दुख की बात है कि शासक वर्ग की बात शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं । जिसका फल यह हुआ कि हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज । वे आगे लिखते हैं ‘धन लोभ ने मानव स्वभाव को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है। कुलीनता और शराफत गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो। साहित्य , संगीत और कला सभी धन की देहरी पर माथा टेकने वाले में हैं। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। डॉक्टर और हकीम है कि वह बिना लंबी फीस के बात ही नहीं करता । वकील और बैरिस्टर है कि वह मिनटों को अशर्फियों में तौलता है। गुण और योग्यता की सफलता उसके आर्थिक लाभ से मापी जा रही है । मौलवी साहब और पंडित जी भी पैसे वालों के बिना पैसे के गुलाम हैं । अखबार उन्हीं की राग अलापते है। इस पैसे ने आदमी के दिल दिमाग पर इतना कब्जा जमा लिया है कि उनके राज्य पर किसी ओर से भी आक्रमण करना कठिन दिखाई देता है। वह दया और स्नेह, सच्चाई और सौजन्य का पुतला मनुष्य दया, ममता शून्य यंत्र बनकर रह गया है। इस महाजनी सभ्यता ने नए – नए नीति नियम गढ़ लिए हैं जिन पर आज समाज की व्यवस्था चल रही है। उनमें एक यह है कि समय ही धन है। पहले समय जीवन था। उसका सर्वोत्तम उपयोग विद्या कला का अर्जन अथवा दीन दुखियों की सहायता थी। अब उसका सबसे बड़ा सदुपयोग पैसा कमाना है ।’ (म.स.69-70) उनकी नजर में ‘किसान परोपकारी है, त्यागी है, परिश्रमी है, किफायती है , दूरदर्शी है, हिम्मत का पूरा है, नियत का साफ है, दिल का दयालु है, बात का सच्चा है, धर्मात्मा है, नशा नहीं करता।’ (विविध प्रसंग भाग 1 पृष्ठ 50) ऐसे किसानों के लिए अथाह प्रेम उनके अंदर है। मुंबई के मजदूरों ने जब हड़ताल की तब उन्होंने उसका समर्थन किया , साथ ही सरकार की इस बात की आलोचना की कि वह मजदूरों का दमन कर रही है।
प्रेमचंद्र महाजनी सभ्यता को सभी बुराइयों की जड़ मानते थे। उनका मानना था कि इर्ष्या जोर जबरदस्ती, बेईमानी, झूठ मिथ्या अभिमान, आरोप, वेश्यावृत्ति , व्यभिचार सभी बुराइयों की जड़ महाजनी सभ्यता है। वे कहते हैं ये सारी बुराइयां तो दौलत की देन है, पैसे के प्रसाद है । महाजनी सभ्यता ने इसकी सृष्टि की है । प्रेमचंद ने 1936 में महाजनी सभ्यता की जो तस्वीर खींची थी वह आज हुबहू साबित हो रही है बल्कि आज उसका रूप और भी विद्रूप और विनाशकारी हो गया। आज हमारे किसान कर्ज के जाल में फंस कर आत्महत्या करने को मजबूर है । खेती आज भी घाटे का सौदा है। गांव उजड़ रहे हैं, किसान मर रहे हैं। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को औने पौने दामों में पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है । शासक वर्ग ने अपने लिए आराम की सारी सुविधा जुटा ली है जनता में त्राहिमाम है ।
प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता के विकल्प में नई सभ्यता की बात की थी। उनका इशारा सोवियत मॉडल की ओर था। आज सोवियत मॉडल अतीत की बात हो गई है। सोवियत संघ का विघटन हो गया है और रुस पूंजीवादी व्यवस्था के अंग बन गया है। लेकिन आज पूंजीवादी दुनिया खुद संकट में फंसती जा रही है। पूरी मानव सभ्यता आज संकट में है। खुद पश्चिमी अमीर पूंजीवादी देशों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोभ और भोग पर आधारित आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और आपदाओं और महामारियों का दौर शुरू हो गया है। कोविड-19 वैश्विक संकट और प्राकृतिक आपदाओं के दौर में इस सभ्यता के भविष्य पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए प्रेमचंद ने प्रेम, सहयोग और सहकारिता पर आधारित जिस नयी सभ्यता की बात की थी वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
अशोक भारत
8709022550
संदर्भ : प्रेमचंद की वैचारिक संवेदना
लेखक : डा. योगेन्द्र, युवा संवाद प्रकाशन, नई दिल्ली – 63
ज़ब्तशुदा कहानियाँ , संकलन एवं संपादन : रामकिशोर
मानवीय समाज प्रकाशन, यवतमाल,(महाराष्ट्र)
वितरक : लोकभारती, इलाहाबाद 211001
प्रेमचंद की चर्चित कहानियाँ
सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी – 221001



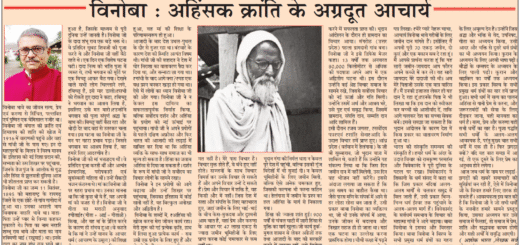
Recent Comments