बैंक : आर्थिक विकास की धुरी
बैंकों के विकास का इतिहास बहुत पुराना है । सभ्यता के विकास के साथ ही बैंकों का भी विकास हुआ है । बैंक शब्द बैनको(Banco ) से निकला है जिसका अर्थ है बेंच पर बैठकर द्रव्य बदलना । प्राचीन काल में विभिन्न देशों( भारत, इटली और यूरोप के अन्य देश) में सोनार या सर्राफ बेंच पर बैठकर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के परिवर्तन का कार्य करते थे, जिससे यात्रियों , परदेशियों और व्यापारियों को सुविधा होती थी । धीरे-धीरे इन सुनारों या सर्राफों में लोगों का विश्वास होने लगा, जिससे लोग इनके पास अपनी बचत और बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षा के लिए धरोहर के रूप में रखने लगे। इन धरोहरों के बदले में वे लोगों को रसीद देते थे तथा उनके संपत्ति सुरक्षित रखने के कार्य के बदले कुछ शुल्क लिया करते थे। ये सर्राफ लोग अपने पास के धन को ऋण के रूप में दूसरों को ब्याज पाने के उद्देश्य दिया करते थे। धीरे-धीरे इन सर्राफों को अनुभव हुआ कि इनके पास लोग जितना धन जमानत के रूप में जमा करते हैं , उनमें से बहुत कम ही निकालते हैं तथा उनकी संपत्ति उनके पास बेकार पड़ी रहती है । अतः सर्राफ उस धरोहर के कुछ हिस्से को कर्ज लगाकर ब्याज के रूप में मुनाफा प्राप्त करने लगे। धीरे-धीरे सर्राफा द्वारा दी जाने वाली रसीदें मुद्रा की तरह प्रयुक्त की जाने लगी । लोग ऋण के लेन-देन में वास्तविक सोने या चांदी का प्रयोग न कर इन्हीं रसीदों से अपना काम चला लेते थे । जैसे-जैसे सर्राफों की ख्याति बढ़ने लगी उनकी रसीदें बैंक नोट की तरह चलने लगी । इस प्रकार, इन्हीं सुनारों तथा सर्राफों के कार्यों से आधुनिक बैंकों का विकास हुआ। बैंकों के ऊपर तीन पीढ़ियां थी व्यापारी ,कर्ज देने वाले महाजन , सोनार या सर्राफा। इस प्रकार धीरे-धीरे बैंकों का विकास हुआ तथा उनका रूप व्यक्तिगत हाथों से निकलकर सम्मिलित पूंजी कंपनी (ज्वाइंट स्टॉक कंपनी) में बदल गई । आधुनिक बैंकों का निर्माण सम्मिलित पूंजी की कंपनी के आधार पर होता है तथा बड़े पैमाने पर उनका व्यापार चलता है।
आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बैंक सन् 1401 में स्पेन के बार्सिलोना नामक शहर में स्थापित किया गया। उसके बाद सन् 1607 में हालैंड में बैंक ऑफ एमस्टरडम की स्थापना की गई। सन् 1619 में जर्मनी में बैंक ऑफ हैम्वर्ग तथा 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई । बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद ही संसार में सम्मिलित पूंजी के बैंकों का विकास हुआ। भारत में सबसे पुराना बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। जून के मध्य सन् 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई। सन् 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ़ बंगाल हो गया। यह प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नमेंट द्वारा स्थापित तीन बैंकों में से एक था । दो अन्य बैंकों में बैंक ऑफ मुंबई जिसकी स्थापना सन् 1840 तथा दूसरा बैंक ऑफ़ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई । तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई जो केंद्रीय बैंक की स्थापना तक केंद्रीय बैंक की भी भूमिका निभाता था । 1935 में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी। आजादी के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हो गया।
भारतीय कम्पनी एक्ट 1949 के मुताबिक बैंक या बैंकिंग संस्था वह कंपनी है जो जनता को उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा को जमा पर प्राप्त करती है तथा इसकी मांग करने पर चेक ड्राफ्ट ऑर्डर अन्य किसी प्रकार से भुगतान करती है।(The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public repayment on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise.- The Indian companies act,1949) हम कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। (Bank is an institution which deals in money and credit)
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग उद्योग निजी हाथों में थे । एक ओर जहां भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इन बैंकों की कोई रुचि नहीं थी , वहीं दूसरी ओर इनका प्रशासनिक एवं विनिमय भी खराब स्थिति में था । इन बैंकों के माध्यम से कुछ उद्योग जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त थे। सन 1947 से 55 के बीच छोटे-बड़े 360 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। इन बैंकों में लोगों की जमा पूंजी डूब चुकी थी । आजादी के बाद देश की आर्थिक स्थिति खराब थी । सरकार के पास पूंजी की बेहद कमी थी। सरकार को लग रहा था कि कमर्शियल बैंक सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे हैं। 14 बड़े बैंकों के पास लगभग 80 फ़ीसदी पूंजी थी। इनमें जमा पैसा उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा था जहां लाभ के ज्यादा अवसर थे । वहीं सरकार की मंशा कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश करने की थी।
भारत में ग्रामीण इलाकों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए तथा समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंकों का समर्थन चाहती थी। लेकिन सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए केंद्र सरकार ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के माध्यम से 14 बड़े बैंकों , जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी, का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बाद में 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कुछ राजनीतिक परिस्थिति भी थी जिसने तात्कालिक सत्तारूढ़ दल को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रेरित किया। जिनका राजनीतिक लाभ उन्हें मिला और उनकी छवि गरीबों के लिए काम करने वाली दल की बनी।
राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग सेवा का विस्तार ग्रामीण इलाकों में हुआ। राष्ट्रीयकरण से बैंकों की स्थिति में भी तेजी से सुधार हुआ । राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों की सिर्फ 8,000 शाखाएं थी जो वर्ष 1994 में बढ़कर 60, 000 तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या 1, 15, 000 के करीब पहुंच गई। इससे पहले सभी बैंक शहरी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्र में 43,000 बैंक स्थापित हो चुके थे । भारत जैसे देश में बैंकिंग व्यवस्था विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए आवश्यक है । राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक भारत में समावेशी विकास एवं विभिन्न कल्याण योजनाओं की धुरी बन गए। वर्तमान में जनधन योजना जैसे कार्यक्रम जिसके अंतर्गत वर्ष 2018 तक लगभग 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए । बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों में काफी पैसा आया जिसे कर्ज के रूप में प्राथमिक सेक्टर कृषि, छोटे उद्योग और छोटे ट्रांसपोर्ट को फायदा हुआ। 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा जो सन् 1969 में 5.7 करोड़ था बढकर 50 साल में 49, 700 करोड़ हो गया । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार , कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (रीजनल रूरल बैंक ) की स्थापना की। देश भर में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 21 हजार से अधिक शाखाएं देश में कार्यरत हैं। कुल 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घटाकर 38 करने की योजना है।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए बैंकों का विलय भी किया गया। बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए नरसिंहम कमिटी और जेपी नायक कमेटी द्वारा विलय के अनुशंसा की गई थी । न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय , 2017 में भारतीय महिला बैंक और पांच अन्य बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय, 2019 में विजया बैंक एवं बैंक देना बैंक का बैंक ऑफ़ बड़ौदा में विलय, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया का पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक , सिंडीकेट बैंक का केनरा बैंक, यूनियन बैंक में आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया है। विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो 2017 में 27 थी अब घटकर 12 हो गई है । विलय से बैंकों के पूंजी आधार सुदृढ़ होगा और जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि होगी । इससे बैंक बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध करने में सक्षम होगा और बैंक ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे बैंकों का फ्रॉड पर भी नियंत्रण होगा।
भारत में बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाता है। विभिन्न माध्यमों से दी जाने वाली सब्सिडी में भ्रष्टाचार और रिसाव की गुंजाइश होती है । इससे बड़ी राशि लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पाती। बैंकों के समावेशीकरण के बाद ऐसी सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से देना संभव हुआ । वर्तमान में गैस सब्सिडी, मनरेगा , किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना , पेंशन , सबके लिए आवास आदि कार्यक्रमों की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में बैंक के माध्यम से देना संभव हो सका है।
आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने के बाद भारत में पहला निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 हुई। इस समय बैंकिंग क्षेत्र में अनेक निजी बैंक कार्य कर रहे हैं, जिनमें एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा , बंधन बैंक आदि लगभग एक दर्जन बैंक शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढी़ है। बैंकों की कार्यदक्षता और ग्राहकों की सेवा में सुधार हुआ है । निजी क्षेत्र के बैंक मूलत: बैंकिंग मूल्यों पर आधारित है और सिर्फ ग्राहक के प्रति जिम्मेदार हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी उत्तरजीविता के साथ-साथ जनता के प्रति सामाजिक , आर्थिक दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, विकास के लिए संसाधन जुटाने तथा सामाजिक समावेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। एक समस्या बैंकों के नियंत्रण को लेकर भी है। सरकार और आरबीआई दोनों बैंकों को दिशा निर्देश देते हैं। इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम काज में सरकारी हस्तक्षेप बढा है और गैर बैंकिंग कार्यों की बढोतरी हुई है। इससे बैंकों की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है।
बैंक के अधिकारी नाम लेने की शर्त पर कहते है कि सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सही आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। सीधा नगद अंतरण के बावजूद लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसमें रिसाव और भ्रष्टाचार है । इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकारी नीति के तहत ऐसे बहुत से काम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों करना पड़ता है जो मूलत: बैंकिंग सेवा के अंतर्गत नहीं आता इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यक्षमता और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
सरकार ने दिशा निर्देश देकर लोन पोर्टफोलियो में 40 फीसदी कृषि लोन की बात की। बैंकों ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए आंख मूंदकर लोन दिया। लेकिन त्रृण वसूली में अपेक्षित सहयोग सरकार और प्रशासन से नहीं मिल पाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकारी नीति, आंतरिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण गैर निष्पादित संपत्ति( एनपीए ) बढ़ रही है ,जो चिंताजनक है । मार्च 2019 में एनपीए का अनुपात 11.2 फीसदी था। परिसंपत्ति का प्रतिफल (रिटर्न ऑफ एसेट) वित्तीय वर्ष 2018 के लिए 0.8 फीसदी, और इक्विटी का प्रतिफल (रिटर्न ऑफ इक्विटी) नकारात्मक था। सरकारी बैंकों में निवेश किए गए प्रत्येक रु का बाजार मूल्य 71 पैसा है जबकि निजी बैंकों में यह पांच गुणा 3.7 रु है। इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत स्थिति में हैं।बाजार के कुल उधारी (क्रेडिट) में उनका हिस्सा 63.2 फीसदी और जमा में 66.9 फीसदी है।
कुछ लोग संकट से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समाधान के लिए निजीकरण का सुझाव दे रहे हैं । भारत जैसे देश में जहां आर्थिक समानताएं मौजूद है, लोगों की स्थिति में सुधार के लिए बैंकिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है । निजीकरण समस्या का समाधान नहीं है । निजीकरण के बुरे अनुभवों के बाद ही सरकार को बाद्घ हो कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। निजीकरण के बजाय सरकार को बैंकों के सेहत सुधारने के लिए आगे आना होगा । गवर्नेंस में सुधार करना होगा । बैंकों का मौजूदा संकट सिर्फ प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं है, बल्कि इसके ढांचे के कारण भी उत्पन्न हुई है। नोट बंदी और कोविड19 के कारण भी बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निजीकरण के बजाय विलय का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।
कोविड-19 के संकट के दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शानदार काम किया है । चाहे लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हो, अथवा कोरोना वायरस के खिलाफ की लड़ाई, बैंक ने अप्रतिम योगदान दिया है । कोरोना कालमें देश की अर्थव्यवस्था के लिए बैंक जीवन रेखा साबित हुआ है। चाहे राहत पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित का सवाल हो या सीधा नगद भुगतान के तहत जनधन खाता , उज्वला योजना , मनरेगा, किसान सम्मान योजना , पेंशन, कृषि सहायता या अन्य कोई योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता सभी सरकारी बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। दुख की बात यह है कि बैंककर्मियों ने अपना जान जोखिम में डालकर करोना वारियर्स के रूप में देश की अहर्निश सेवा की है लेकिन उनको वह स्वीकृति सरकार या समाज से नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। गौर करने लायक बात यह है कि की कोराना वायरस के खिलाफ की लड़ाई में सरकारी स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक बैंक ही लोगों के काम आए हैं। इसलिए इनका सार्वजनिक स्वरूप बनाए रखना देश हित में है।
अशोक भारत
मो. 8709022550


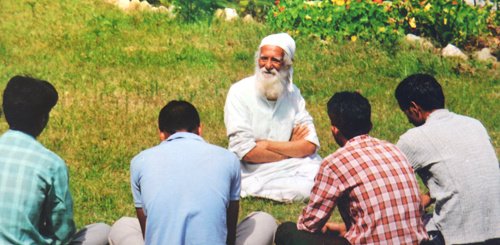
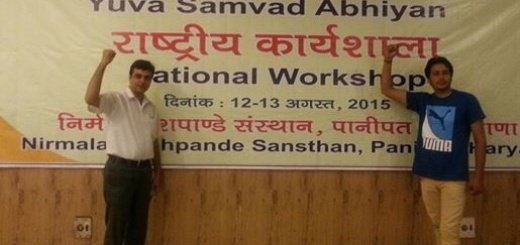
Recent Comments