गंगा : एक आैर भगीरथ की तलाश है
– अशोक भारत
करोड़ो लोगों के धार्मिक आस्था और विश्वास का केन्द्र तथा आजिविका का आधार जीवनदायिनी गंगा आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी और विकसित हुई हैं लेकिन आधुनिक सभ्यता नदियों को मार रही है। गंगा को लेकर चिंताए बढ रही है। समाधान की पहल भी हो रही है। फिर भी समस्याएं विकराल होती जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि ‘ मॉ गंगा ने बुलाया है।’ चुनाव के बाद उन्होने ‘नमामि गंगा योजना’ की शुरूआत भी की। इसके लिए अलग मंत्रांलय बनाया और मंत्री की नियुक्ति की। बजट में इसके लिए अगले पॉच वर्ष के लिए २०,००० करोड़ का प्रवधान भी किया। थोड़ा पीछे जाए तो पाते है कि १९८६ में तात्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने गंगा कार्य योजना की शुरूआत की थी। जिसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार लाना था। नवम्बर २००८ में केन्द्र की यू पी ए सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और फरवरी २००९ में राष्ट्रीय गंगा घाटी प्रधिकरण का गठन किया गया। जिसका लक्ष्य २०२० तक गंगा में किसी भी प्रकार के असंसाधित गंदे पानी तथा औद्योगिक बहिस्राव को बहने नहीं देना है। गंगा घाटी में जल-मल, औद्योगिक प्रदूषण , नदी अग्रभाग के विकास आदि पर कार्ययोजना बनाना तथा गंगा की अविरलता एवं निर्मलता को सुनिश्चित करना है, और अब नमामि गंगे योजना शुरू की गई है। इन सरकारी प्रयासों और योजनाओं पर अरबों रूपया खर्च हो चुके हैं। अरबों रूपया लुटाने के बाद गंगा आज मरणासन्न स्थिति में पहुंच गयी है, तो सवाल उठना लाजिमी है चूक कहां हुई ? योजना में या उसके क्रियान्वयन में? गंगा की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन ?
मध्य हिमालय में स्थित उत्तराखण्ड अपने नैर्सगिक सैन्दर्य एवं धार्मिक विश्वास के लिए विश्वविख्यात है । छोटी-बड़ी पर्वत मालाएं,नाना प्रकार के पेड़-पौधे वनस्पति,जीवनदायिनी जड़ी-बूटियां क्रीड़ा करते अनेक प्रजाति के पशु,कलरव करते नाना प्रकार के पक्षी आदि इसकी खासियत है। हिमाच्छादित पर्वत चोटियों से निकलने वाली नदी गंगा गोमुख से २५१० कि.मी. की यात्रा कर गंगा सागर में समुद्र में समा जाती है । उत्तराखण्ड में दो महत्त्वपूर्ण घाट है भागीरथी और अलकनन्दा। भागीरथी, भीलंगना, बालगंगा और असि की कुल लम्बाई ४५६ कि.मी.।अलकनन्दा, मंदाकिनी, नन्दाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, बिदरीगंगा आदि छोटी नदियों की लम्बाई ६६४ कि.मी. है। यानी दोनो घाटी की कुल लम्बाई ११२० कि . मी. है। इन्ही घाटियों में स्थित है पंच प्रयाग जिससे करोड़ों लोगों की आस्था एवं विश्वास जुड़ी है। धौलीगंगा और विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। विष्णुप्रयाग को अलकनन्दा भी कहते है। नन्दप्रयाग में नन्दाकिनी का अलकनन्दा में संगम होता है। उत्तरवाहिनी पिंडर और अलकनन्दा का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। रूद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनन्दा का मिलन होता है। गोमुख से निकलनेवाली भागीरथी तथा हिमनद से निकलनेवाली अलकनन्दा का संगम देव प्रयाग में होता है।यही गंगा अपना नाम और स्वरूप प्राप्त करती है।
गंगा मुख्यत: हिम पोषित नदी है। एक आकलन के अनुसार गंगा के बहाव का ७० प्रतिशत हिमनद के कारण है। लेकिन पर्वतों पर मानव क्रियाकलापों में वृद्धि, विलासी पर्यटन, यात्रियों की अत्यधिक आवागमन , होटल, बाजार आदि के कारण कार्बन कणों में वृद्धि से हिमनद तेजी से पिघल रहें हैं। मिट्टी के तेल, डीजल, यात्री वाहन, गोबर, सुखी वनस्पति, वन अग्नि काण्ड से हिम शिखाओं पर कार्बन जम रहे हैं, जो इनके पिघलने का मुख्य कारण है। एक अमेरिकी शोध संस्थान के आकलन के अनुसार २०४० तक हिम शिखाएं पूरी तरह अदृश्य हो सकती हैं , अगर सबकुछ इसी प्रकार चलता रहा तो। अगर हिम शिखाओं को बचाने के प्रयास नहीं किए गए तो गंगा बचाने की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। ऱाष्ट्रीय गंगा धाटी प्राधिकरण की योजनाएं एवं नमामि गंगे योजना इस विषय पर मौन है। सरकार की योजना में हिम शिखर को बचाने की योजना का शामिल न होना विस्मयकारी और पूरी योजना के आधे-अधूरेपन का एहसास कराता है।
हिमालय के घने जंगल ही पहाड़ से उतरनेवाली गंगा के वेग को नियंत्रित करता है। लेकिन सोपानी बांधों (cascading dams) और कथित विकास के नाम पर जंगलों की तेजी से कटाई हो रही है. उतराखण्ड में २००० और २०११ के बीच में ४७५६ वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र कम हुआ है, जो राज्य कुल वन क्षेत्र (५३४८३ वर्ग कि मी) का ९ फीसदी है। देश में प्रतिवर्ष १८००० वर्ग कि मी स्वभाविक वन कृतक(monoculture) वनों में परिवर्तित हो रहा है। १२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र को अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित किया गया है। गंगोत्री के आसपास देवदार के घने जंगल मौजूद हैं लेकिन विकास की कुदृष्टि उनपर भी पड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए ८००० देवदार के पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। गांव वाले चाहते है कि पेड़ों की कटाई रूके। आर्मी ने भी एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया जिसमें सिर्फ ६०० पेड़ काटने पड़ते ।मगर योजनाकारों को यह सुझाव रास नहीं आया। गॉव वाले शंका जाहिर करते है कि एक बार पेड़ों की कटाई शुरू हो गयी तो यह संख्या ८००० पर ही रूकेगी इसकी कोई गारन्टी नहीं है .
भागीरथी घाटी में कुल ३२ बांध हैं. इनमें ९ में कार्य प्रारम्भ है, ४ निर्माणाधीन और १९ प्रस्तावित है। अलकनन्दा घाटी में ८ बांध प्रारम्भ है, १० निर्माणाधीन और २० प्रस्तावित है, कुल ३८ बांध है। वैसे उत्तराखण्ड में बांधों को लेकर अलग-अलग एजेंसियों के आकडे भिन्न-भिन्न है। सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां कुल ५८० बांध प्रस्तावित, निर्माणाधीन या कार्यरत हैं। भागीरथी नदी की परयोजना में शामिल है : भैरोघाटी पनबिजली स्कीम भाग-१ (३२४ मेगावाट), भैरोघाटी पन बिजली स्कीम भाग-२, लोहारी नागपाला पन बिजली(५२० मे.) पालामनेरी पन बिजली (४१६) , मनेरीभाली पन बिजली भाग-१ (९० मे. ) मनेरी भाली भाग-२ (३०४ मे.) , टिहरी बांध परियोजना ( १००० मे .), कोटेश्वर (४० मे .) आदि अलकनन्दा एवं सहायक नदियों की परियोजना में शामिल हैं विष्णुप्रयाग (४०० में.), तपोवन विष्णुगाड (५२० मे.), श्रीनगर ( ३३०) , सिंगरोली भटवारी(९९ मे.) ,कोटली भेल-२ ( ५३० मे.) आदि। चिल्ला (१४४ मे.) टिहरी ( १०००), मनेरी भाली-१ (९० मे. ), मनेरी भाली-२( ३०४ मे.) , विष्णुप्रयाग ( ४०० में ) आदि कार्यरत परियोजनाएं है। निर्माणाधीन परियोजना में शामिल है काली गंगा-१, काली गंगा-२, कोटेश्वर, कोटली भेल-१ए, कोटली भेल- १बी , कोटली भेल-२, तपोवन विष्णुगाड, पालामनेरी, मदमहेश्वर, लोहारीनागपाल, श्रीनगर, सिंगरौली भटवारी आदि। कुल ४१ परियोजनाएं।
भागीरथी तथा अलकनन्दा घाटी की नदियों की कुल लम्बाई ११२० कि मी है, जिनमें ५६२ कि मी यानी ४७ प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों तथा सुरंग द्वारा प्रभावित है। उन सभी बांधों के लिए १६०० कि मी सुरंग खोदी गई है। इतना होते हुए भी निर्माण कार्य करना अभी शेष है। इसका मतलब है उत्तराखण्ड में नदियों की तुलना में जलासयों का क्षेत्र अधिक होगा और नदी की लम्बाई से ज्यादा सुरंगों की लम्बाई होगी। अगर प्रस्तावित और निर्माणाधीन बांध बन जाय तो हर १.५ कि मी पर एक बांध होगा सोपानी बांधों के कारण मछलियों के पथ अवरूद्ध होते हैं उनका प्रजनन प्रभावित होता है । गाद संचय में वृद्धि के कारण जल की गुणवत्ता बिगड़ती है और जैव विविधता प्रभावित होती है।तलछट में घटाव से बाढ के क्षेत्र में इजाफा होता है और नदी घाटी के आकार में परिवर्तन होता है।खेतों में उपजाऊ मिट्टी की कमी से रसायनिक खाद पर निर्भरता बढ जाती है। समुद्र तटों का क्षरण अधिक होता है पिछले बीस वर्षों में गंगासागर का धबलाता गांव का १.५ कि मी सागर ने निगल लिया है।
जलाशय का स्थगित पानी जैविक पदार्थों को संग्रहित करता है और मिथेन जैसी विषैली गैस का निर्माण करता है। वह विद्युत उत्पादन गृह में जल में मिलती है और वहॉ से वातावरण में धुल जाती है। अलकनन्दा की बांधों की परियोजना से पंच प्रयाग डूब जाएगा। और इसके साथ ही विकास की बलिवेदी पर डूब जायेगा हजारों साल से चली आ रही असंख्य लोगों की धार्मिक आस्था एवं विश्वास का केन्द्र कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार पूरा टिहरी गांव डूब गया विकास ( विनाश) की आंधी में। जलाशयों के स्थगित जल भूस्खलन को बढाते है। नदियों के नीचे भी जल की एक धारा बहती है। नदियों के बहाव पर बांध एवं दिशा परिवर्तन से निचली धारा का बहाव प्रभावित होता है । वे जल की गुणवत्ता, तापमान, संचलन, जलचरों, वन्य जीवों तथा आजिविका ( जिनकी आजिविका नदी प्रणाली पर आधारित है ) पर प्रभाव डालते है। नदी का न्यूनत्तम पर्यावरणीय बहाव कितना हो यह आज तक तय नहीं है। गैर मानसून महीने में बहाव १०-१५ फीसदी माना गया है यह ठीक नहीं है । स्रोत संरक्षण के साथ स्रोत उपयोग में संतुलन ही समाधान है।
हिमालय नया पहाड़ है जो अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। यह भूकम्प वाला क्षेत्र ४ और ५ की श्रेणी में आता है। इसलिए यहां भूकम्प के छोटे-बड़े झटके आते ही रहते हैं। जिससे भूस्खलन होता रहता है। वनों के विनाश से पहाड़ नग्न हो गया है । भूस्खलन बढ गया है। कम घने वनों एवं मानव क्रिया-कलापों का परिणाम अनेक समस्याओं के रूप में सामने आया है – जैसे अधिक भूस्खलन, नदियों में अधिक तलछट, बांध/ जलाशय का अल्पावधि और नदियों में उच्चत्तर गदलापन आदि।
जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ों पर तबाही के कारण बन रहे हैं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने भी माना है। जून २०१३ में आयी आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने माना कि श्रीनगर शहर के जो हिस्से मलवे में दवे वह मलवा २६ से ४३ प्रतिशत श्रीनगर बांध की मक थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विष्णु प्रयाग बांध नहीं होता तो उपड़ से बांध के साथ लगा मलवा बिना रुकावट के बह जाता और इतनी तबाही नहीं होती। श्रीनगर इसका बड़ा कारण है। दरअसल बांध निर्माण से निकला मक और मलवा नदियों के स्वास्थ्य के लिए गम्मभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। बांध कम्पनी मक व मलवा को नदी के किनारे या सीधे नदी में डाल देती है, ताकि ये नदी में ही बह जाय और बांध कम्पनी को सुरक्षा दीवारे बनाने या मक को नदी में बहने से बचाने संबंधी अन्य कार्य करने का खर्च बच जाय।जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नदी में मक बहाने पर पाबंदी है।
भागीरथी-गंगा की स्थिति यह है कि मनेरी भाली चरन १ एवं २ के नीचे गंगा नदी सूखी है तो कोटेश्वरऔर टिहरी बांध के नीचे रेत का अम्बार या झील का ठहरा हुआ पानी है और उसकी गंदगी है। गंगा की सफाई पर योजना बनाने वाले उपक्रमों के तहत चाहे नमामि गंगे हो ,स्पर्श गंगा हो या स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा के मायके में गंगा की बांधो से क्या तबाही हुई है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि ये नदी की जैविक प्रणाली और पारिस्थितिकी को पूरी तरह से प्रभावित करती है। २०१० में टिहरी झील भरने के कारण झील के किनारे के ४५ गांव धंसने लगे थे। बांध कम्पनी ने (टी एस डी सी) उन्हे बांध से प्रभावित नहीं माना । फिर सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमा ( एन डी जुयाल , शेखर सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य) के दबाव में सरकार उनके लिए एक नीति बनाने के लिए बाध्य हुई। इन बांधों से संबंधित अभियंत्रिकी या सर्वे कितना गलत है उसके कई उदाहरण सामने आए हैं। मनेरी भाली चरण २ के बाद जब उसमें पानी भरा गया तो मालूम पड़ा कि उत्तरकाशी के गंगा किनारे के दोनो हिस्से जोशियाडा और ज्ञानसू डूब में आ रहे हैं। लोगों को घर छोड़ कर बाहर रहना पड़ा और जून २०१३ में ये हिस्से टूट कर बह गए। बांध बनाने के बाद मनेरी भाली चरण २ का विद्युत गृह टिहरी झील में आ गया। विष्णुप्रयाग बांध की सुरंग के उपड़ बसे चाई और थैंग गांव बरसो बाद अचानक धस गए । टिहरी झील के कारण विस्थापितों की संख्या बढती ही जा रही है। गंगा तो अपने मैके में कैद है जब तक उसे इस कैद से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक गंगा सफाई की सारी योजनाएं एवं कार्यवाही निष्फल साबित होंगी। अविरलता के बिना निर्मलता संभव नहीं है चाहे हम उसके लिए जितना धन खर्च करें। गंगा कार्य योजना की विफलता इसके उदाहरण है।
सोपनी बांधों एवं सुरंग से निकलकर गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाका में प्रवेश करती है।हरिद्वार से गंगा सागर तक की यात्रा एक त्रासदी से कम नहीं है। हरिद्वार से कन्नौज पहुंचते-पहुंचते गंगा का गला घुट जाता है। सारा पानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की प्यास बुझाने में खप जाता है। और गंगा में बच जाता है सहायक नदियों एवं नालों का पानी। सहायक नदियां अपने साथ प्रदूषण की भारी खेप भी लाती हैं। गंगा के किनारे शहरों से प्रतिदिन ३००० एम एल डी सीवेज निकलता है जिसके एक तिहाई यानी १००० एम एल डी का ही शोधन एस टी पी में होता है। बाकी सीधे नदी में पहुंचता है। १३८ नालों का गंदा पानी गंगा में पहुंच रहा है। गंगा किनारे कुल ७६४ कल-कारखानें हैं जिसमें रसायन डिस्टिलरी,डेयरी, पल्प और पेपर, चीनी, टेनरी,टेक्सटाइल्स,बलीचिंग, सिमेन्ट,पेट्रोकेमिकल्स,कीटनाशक आदि के कारखाने शामिल हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ६८७ कल- कारखानें हैं जिनमें ४४२ तो चर्म उद्योग के हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड में ४२, बिहार में १३ और बंगाल में २२ कारखानें हैं। ये कारखाने ७० प्रतिशत प्रदूषित जल गंगा में गिराते है। गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण मल- जल और कारखानों से निकलनेवाला विषाक्त कारक है। इन कारखानों में लेड,कैडियम,क्रोमियम,निकेल,कॉपरआदि जहरीली धातु होती है। वर्तमान ट्रीटमेन्ट प्लान्टों में इन्हें दूर करने की व्यवस्था नहीं है।
नदी मामले के विशेषज्ञ मानते हैं कि गंगा के किनारे जो दिख रहा है उसका प्रभाव गंगा बेसिन पर भी पड़ रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि खेती खत्म होगी और तमाम तरह के बीमारियों का दौड़ शुरू होगा, क्योकि ट्रीटमेंट आदि का स्वांग पूरी तरीके से अवैज्ञानिक नजरिए के साथ चल रहा है। गंगा के कारण दो करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। गाजीपुर, बलिया आदि इलाके में आर्सेनिक पट्टी बननी शुरु हो गयी है । इन इलाके के लोग आर्सेनिक से बने बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। इनमें दांतों का पीला होना, दृष्टि कमजोर पड़ना, बाल जल्दी पकने लगना,कमर टेढी होना और त्वचा संबंधी बीमारी प्रमुख है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय का मानना है कि कानपुर से आगे बढने पर वराणसी, आरा, पटना, मुंगेर से लेकर फरक्का तक आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित सीमा से १० से १५ प्रतिशत तक ज्यादा है । यह इसलिए कि गंगा में तकरीबन तीन सौ करोड़ लीटर प्रदूषित कचरा रोज गिर रहा है। विश्वबैंक की एक रिपोट बताती है कि उत्तर प्रदेश की १२% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। कैंसर पर भारत में शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने सन् २०१२ में पाया कि भारत में कहीं भी कैंसर कई रूप उतने व्याप्त नहीं हैं जितने गंगा के इलाके मे , खासकर उ प्र, बिहार और बंगाल में।पाप धोने वाली पवित्र गंगा को हमने जानलेवा रोगों का स्रोत बना दिया है।
बिहार के कहलगांव से सुलतानगंज तक ८० कि मी लम्बे पट्टी को डाल्फिन सेन्चुरी घोषित किया गया है। सेन्चुरी में फिलहाल १७०-१९० डॉल्फिन बची है। पूरे देश में करीब २५०० डॉल्फिनें बची हैं। इनमें १००० के करीब गंगा में है और उनमें भी ६० प्रतिशत बिहार वाले इलाके है। डॉल्फिन को गंगा के स्थास्थ्य का सूचक भी माना जाता है। इसको देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि गंगा जल की स्थिति क्या है। डॉल्फिन सेन्चुरी घोषित होने के बाद कहलगॉव से सुलतानगंज तक मछली मारने पर प्रतिबंध है। उल्लेखनीय है कि करीब तीन दशक पूर्व मछुआरों ने गंगा मुक्ति आन्दोलन चला कर जलकर जमींदारी से मुक्ति पायी और मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त किया। अब डॉल्फिन सेन्चुरी के कारण मछुआरों के रोजगार खत्म हो गए है ।गंगा मुक्ति आन्दोलन के नेता अनिल प्रकाश कहते है कि गंगा के प्रदूषण ने कई डेड जोन बनाए है जिसके चलते ७५% मछलियां समाप्त हो चुकी है। पहले बिहार में मछुआरे गंगा से ४७ प्रकार की मछलिया पकड़ते थे। लेकिन प्रदूषण और फरक्का बराज के कारण इनका रोजगार चौपट हो गया है और रोजगार की तलाश में उन्हे दर-दर भटकना पड़ता है। फरक्का बराज के कारण गंगा में हिलसा एवं झिंगा मछलियों का आना बंद हो गया है।
फरक्का बराज के कारण बाढ एवं काटाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसके समाधान की पहल नहीं की गयी तो यह विकराल रुप धारन कर लेगा जिन्हे सम्भालना आसान नहीं होगा। दरअसल फरक्का बराज नदी के साथ प्राकृतिक रुप से बहनेवाली बालू और मिट्टी को रोक रहा है। इसके कारण गंगा में रेत के टापू बन रहे हैं। इन टपूओं के कारण गंगा बाढ के दिनों में काटाव करती है और गॉव का गॉव साफ हो जाते है। बंगाल के मालदा जिला के पंचाननपुर का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। बराज से लगभग ६ कि मी की दूरी पर बसा गॉव सिमलतल्ला का भी कोई अस्तित्वनहीं है जो हजारों घरों वाला गॉव हुआ करता था।फरक्का बराज के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बाढ और कटाव का प्रकोप बढ रहा है। जब यह बराज नहीं था तो हर साल बरसात की पानी की तेज धारा के कारण १५० से २०० फीट तक गंगा की उड़ाई हो जाती थी। बराज के कारण यह प्रक्रिया रूक गई है और नदी तल उपड़ उठता गया है। सहायक नदियों की भी उड़ाई प्रक्रिया रूक गयी है। इसके परिणामस्वरुप जल जमाव के क्षेत्र भी बढने लगे है़ं। बराज के कारण पॉच लाख से अधिक लोग अब तक अपनी जमीन से उखड़ चुके हैं और बंगाल के मालदा एवं मुर्शिदाबाद जिला के ६०० वर्ग कि मी उपजाऊ भूमि गंगा में विलीन हो चुकी है। १९७५ में जब यह बराज बना था तो मार्च के महीने में ७२ फीट पानी रहता था। अब यह गहराई घट कर १२-१३ फीट रह गई है। दरअसल दूरगामी दृष्टिकोण से देखे तो फरक्का बराज के कारण उत्पन्न दुष्परिणाम इसके लाभ से अधिक प्रतीत होते हैं। इसलिए आज फरक्का बराज पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसके बिना गंगा की अविरलता और निर्मलता की किसी कार्ययोजना का कामयाब होना संम्भव नहीं है।
आजकल नदी के पानी का उपयोग मुख्यत: तीन कार्य के लिए हो रहा है। पहला पीने के पानी , दूसरा कृषि कार्य और तीसरा उद्योग के लिए। इसमें नदी का लगभग ८० प्रतिशत पानी चला जाता है। यही पानी जहरीला बनकर फिर नदी में पहुंचता है। पहले नदी गॉव के नीचे बहती थी । नदी के किनारे तालाब होता था। इससे ये तीनो कार्य होते थे। थोड़ा पानी कम पड़ गया तो नदी से लिया जाता था। बाढ के समय ये तालाब भर जाते थे। गैर मौनसून के दिनों में पानी रिसकर नदी में पहुंचता था। इसका एक लाभ यह होता था कि तालाब भूजल के स्तर को कायम रखते थे। विकास की आपाधापी में हमने पीढियों से आ रही जल संचय का वैज्ञानिक तरीका छोड़ दिया है। हम पूरी तरह से नदी पर निर्भर होते जा रहे हैं।यह दौड़ बड़ी नदियों से जल हरणे और उसी अनुपात में गंदगी मिलाने का है। आनेवाली पीढियों को भी बिजली की आवश्यकता होगी, इसकी चिंता नहीं है। नदियों को अधिकतम निचोड़ कर बल्व जलाने ,अपने कारखाने चलाने और अपने खेतों में सिंचाई करने को ही हम विकास की योजना मान चुके है। इनमें सभी सरकारें एकमत दिखती हैं।
विकास की पश्चिमी उपभोक्तावादी मॉडल के कारण मानव सभ्यता आज संकट में है. अगर हमें अपने तथा आनेवाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना है, तो महात्मा गाँधी के इस कथन को ध्यान रखना होगा कि हमारी सारी आवश्यकताएँ पूर्ति करने का सामर्थ पृथ्वी को है मगर एक भी आदमी का लालच पूरा करने का सामर्थ इसमें नहीं है. इसको ध्यान में रखते हुए जो योजना बनेगी उसीसे हम हिमालय और नदियों को बचा सकते हैं. हिमशिखर ( glacier) को बचाने के लिए हिमनदी मुख से १५० कि मी तक के इलाके को संवेदनशील घोषित किया जाय। विभिन्न क्रियाकलापों विशेषकर विलासी पर्यटन पर प्रतिबंध लगा दिया जाय। चार धाम से १५० कि मी का दूर तक का परिसर संवेदनशील घोषित करना चाहिए। कोई भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप और भारी निर्माण न हो। पहाड़ो पर १००० मी से अधिक ऊँचाई पर पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगाना चहिए। वन अग्नि को रोकने के उपाय करने चाहिए। पर्यटनकों के वाहनों पर निंयंत्रण, जलाऊ लकड़ी, मिट्टी के तेल, वाहन ,कूड़ा करकट, और त्याज्य वस्तुओं को जलाना बंद करना चाहिए। तापमान बढाने वाले विद्युत उपकरनों, पर्यटन वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। धुआं रहित चूल्हों, प्रेशर कुकरों, गैस स्टोव के लिए प्रोतसाहन देना चाहिए। पुरातन चूल्हों को धुआं रहित स्वच्छ चूल्हों में परिवर्तन करना चाहिए।
मैदानों में वनो की कटाई से पहाड़ की ओर चलनेवाली गर्म हवा पर्वतीय तापमान को बढाते है़ं। इसे रोकने के लिए मैदानी इलाके में भी वन लगाना चहिए। अलकनन्दा, मंदाकिनी और भागीरथी पर बांध नहीं बनाने चहिए। भीमगौड़ा और अन्य नहरों के माध्यम से गंगा जल दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। गंगा बेसिन में वर्षा जल संचय एवं भूजल पुनर्भरण योजनाओं को कड़ाई से लागू करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है खेतों के मेड़ की ऊचाई कमसे कम आधा मीटर करना चहिए।नदी मामलों के विशेषज्ञ प्रो यू के चैधरी कहते है कि पारिस्थितिकी आकडे़ उपलब्ध नहीं है। बिना आकड़े के गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का सपना देखा जा रहा है। मसलन घाट कहॉ बनना चाहिए इसका अध्ययन नहीं है, भूजल स्तर कितना गिर रहा है और बालू क्षेत्र का कितना विस्तारित हुआ है किसी चीज का कोई आकड़ा नहीं है। ३०% से अधिक जल का दोहन नहीं होना चाहिए। अभी यह ९५% है। गंगा बेसिन प्राधिकरण के संस्थापक सदस्य एवं नदी मामले के विशेषज्ञ प्रो बी डी त्रिपाठी का मानना है कि सतस प्रवाह की योजना यदि लागू नहीं की जाती तो नमामि गंगे योजना सफल नहीं होगा।सरकार की योजना प्रदूषण नियंत्रण पर केन्द्रित है जबकि आवश्यकता गंगा में अविरला की अधिक है। सिंचाई के तौर-तरीकों में बदलाव की भी जरूरतहै। हमें कम पानी खपत वाली सिंचाई नीति और तकनीक अपनानी चाहिए।
नदियों का भी अपना स्वधर्म होता है. स्वधर्म यानी स्वभाव, नदी का स्वभाव है बहना. इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना प्रकृति के साथ विद्रोह है, कुदरत के कानून का उल्लंघन है. लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ विनाश को निमंत्रण देना है. हिमालयी क्षेत्र में होने वाले हलचल, जलवायु परिवर्तन एवं उसके उत्पन्न समस्याएं इसी ओर इशारा करते है. अगर इससे बचना है तो प्रकृति के साथ साम्य स्थापित कर जीना सीखना होगा. पिछले चालीस पचास सालों में गंगा बहुत बुरे दौड़ से गुजर रही है। विकास की नई अवधारणा के कारण ही यह संकट उत्पन्न हुआ है। विकास के मैजूदा अवधारणा को बदले बिना हम गंगा को नहीं बचा सकते। हमें अपने सोच में बुनियादी और रचनात्मक परिवर्तन करना होगा। अगर गंगा को बचाना है तो गोमुख से गंगा सागर तक सम्पूर्ण गंगा बेसिन के लिए एक मुकम्मल योजना और उसे लागू करने के लिए दृढ इच्छा-शक्ति का होना जरूरी है। क्या हम इस भगीरथ प्रयत्न के लिए तैयार हैं?
अशोक भारत
bharatashok@gmail.com
Mob – 8004438413

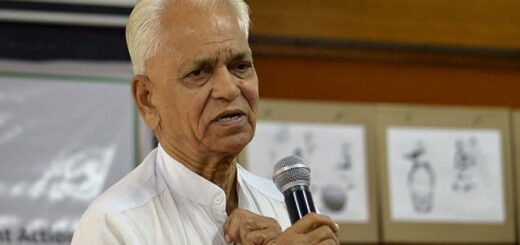

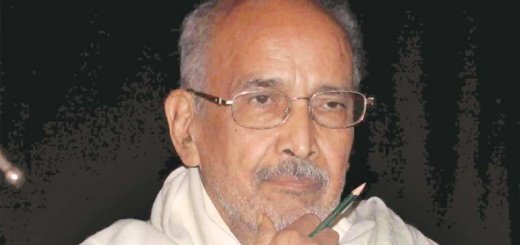
Recent Comments