गांधी : भविष्य का महानायक
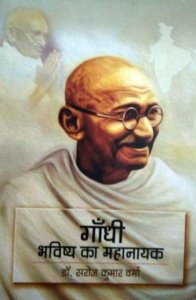 महात्मा गांधी विश्व के उन विरले सत्पुरुषों में हैं जिनपर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है , और लिखी जा रही हैं। जो अपने आप में गांधी के जीवन, विचार और कार्यों की प्रासंगिकता पर बड़ी टिप्पणी है। गांधी पर लिखी गई पुस्तकों की कड़ी में कवि एवं दर्शनशास्त्र के अचार्य डॉ.सरोज कुमार वर्मा की नई किताब “गांधी : भविष्य का महानायक” प्रकाशित हुई है, जो दर्शन की कसौटी पर गांधी को समझने एवं परखने का भी प्रयास है। यह पुस्तक वस्तुतः लेखक के शोधपरख आलेखों का संग्रह जो अलग-अलग काल खंड में लिखा गया है । इस पुस्तक में मुख्यत: दो खंड है । पहला स्वतंत्र खंड और दूसरा तुलनात्मक खंड । स्वतंत्र खण्ड में हिंद स्वराज : गांधी का सभ्यता दर्शन , भूमंडलीकरण के युग में गांधी का सर्वोदय: औचित्य की तलाश , गांधी चिंतन में पर्यावरण चिंता तथा गांधी का सत्याग्रह : मानव अधिकारों के मात्रात्मक संरक्षण की प्रविधि चार आलेख शामिल हैं। दूसरे खंड में भी चार महत्वपूर्ण आलेख हैं। दूसरा खंड तुलनात्मक अध्ययन का है ।इसमें महावीर और गांधी की अहिंसा : एक तुलनात्मक अध्ययन, विवेकानंद और गांधी का सभ्यता चिंतन : एक तुलनात्मक अध्ययन, टैगोर और गांधी का ईश्वर विचार : एक तुलनात्मक अध्ययन तथा श्री अरविंद और गांधी का शिक्षा दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन शामिल है , जो आमतौर पर गांधी विचार की किताबों में देखने को नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक इस मायने में थोड़ा लीक से हटकर है । यह पुस्तक जिज्ञासु पाठकों एवं शोधार्थियों के लिए संग्रहनीय तो है ही साथ ही साथ गांधी विचार में रूचि रखने वाले सामान्य जनों के लिए भी उपयोगी है।
महात्मा गांधी विश्व के उन विरले सत्पुरुषों में हैं जिनपर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है , और लिखी जा रही हैं। जो अपने आप में गांधी के जीवन, विचार और कार्यों की प्रासंगिकता पर बड़ी टिप्पणी है। गांधी पर लिखी गई पुस्तकों की कड़ी में कवि एवं दर्शनशास्त्र के अचार्य डॉ.सरोज कुमार वर्मा की नई किताब “गांधी : भविष्य का महानायक” प्रकाशित हुई है, जो दर्शन की कसौटी पर गांधी को समझने एवं परखने का भी प्रयास है। यह पुस्तक वस्तुतः लेखक के शोधपरख आलेखों का संग्रह जो अलग-अलग काल खंड में लिखा गया है । इस पुस्तक में मुख्यत: दो खंड है । पहला स्वतंत्र खंड और दूसरा तुलनात्मक खंड । स्वतंत्र खण्ड में हिंद स्वराज : गांधी का सभ्यता दर्शन , भूमंडलीकरण के युग में गांधी का सर्वोदय: औचित्य की तलाश , गांधी चिंतन में पर्यावरण चिंता तथा गांधी का सत्याग्रह : मानव अधिकारों के मात्रात्मक संरक्षण की प्रविधि चार आलेख शामिल हैं। दूसरे खंड में भी चार महत्वपूर्ण आलेख हैं। दूसरा खंड तुलनात्मक अध्ययन का है ।इसमें महावीर और गांधी की अहिंसा : एक तुलनात्मक अध्ययन, विवेकानंद और गांधी का सभ्यता चिंतन : एक तुलनात्मक अध्ययन, टैगोर और गांधी का ईश्वर विचार : एक तुलनात्मक अध्ययन तथा श्री अरविंद और गांधी का शिक्षा दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन शामिल है , जो आमतौर पर गांधी विचार की किताबों में देखने को नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक इस मायने में थोड़ा लीक से हटकर है । यह पुस्तक जिज्ञासु पाठकों एवं शोधार्थियों के लिए संग्रहनीय तो है ही साथ ही साथ गांधी विचार में रूचि रखने वाले सामान्य जनों के लिए भी उपयोगी है।
जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट है गांधी वर्तमान के महानायक तो हैं ही , वे भविष्य के भी महानायक है । इस स्थापना को बहुत ही मजबूती से तथ्यों ,तर्कों और दर्शन की कसौटी पर स्थापित करने का सफल प्रयास लेखक ने इस पुस्तक में किया है। अपनी बात के समर्थन में लेखक ने गांधी के तल्ख आलोचक ओशो( रजनीश) को उद्धृत किया है। ओशो कहते हैं “गांधी को दुनिया के उन थोड़े से महापुरुषों में से एक मानता हूं जो पत्थर की प्रतिमा की तरह है। जिन पर वर्षा होती है और धूल बह जाती है , प्रतिमा और निखर कर प्रगट होती है । यह निखार उत्तरोत्तर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि गांधी ने मानव मुक्ति का जो पैगाम दिया है उसे सुनकर हर काल में बंदी मानवता न सिर्फ मुक्ति के लिए संघर्ष करेगी बल्कि जीतकर मुक्त भी होगी।”
हिंद स्वराज गांधी विचार को समझने की सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य पुस्तक है । इसलिए इस पुस्तक में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लेख हिंद स्वराज्य : गांधी का सभ्यता दर्शन है । लेखक का मानना है कि “हिंद स्वराज में आज भी कुछ बदलने लायक नहीं है । ताज्जुब होता है कि किसी व्यक्ति में ऐसी दूर दृष्टि कैसे हो सकती है? कैसे कोई सौ साल बाद आने वाले भविष्य को इतनी स्पष्टता से देख सकता है कि तब की कही हुई बात अब अक्षरश: साबित हो। मगर गांधी ऐसे ही थे। इतिहस को अपने इशारों पर बदलने वाले । भविष्य को अपनी उंगलियों से सँवारने वाले । इसलिए उन्होंने अपने सभ्यता दर्शन को हिंद स्वराज को केंद्र में रखकर उसकी परिधि पर घटने वाली घटनाओं की चर्चा की है। वह आज हू- ब- हू घटित हो रही है । इसलिए यह छोटी- सी पुस्तिका उस वक्त जितनी जरूरी थी उससे ज्यादा जरूरी इस वक्त हो गई है , क्योंकि इसमें बताए हुए रास्ते पर चलने के सिवाय मानव मुक्ति का और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ”
हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्वराज्य , राष्ट्र , धर्म , मशीन , शिक्षा, सत्याग्रह, आधुनिक औद्योगिक सभ्यता आदि समग्र विषयों पर अपनी स्पष्ट एवं बेबाक बात रखी है, जिस पर वह अंत तक कायम रहे। यह भी एक विडंबना है कि गांधी जी ने जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और जिसे उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया था उन दोनों ने ‘ हिंद स्वराज’ को सिरे से खारिज कर दिया था। फिर भी यह पुस्तक सौ साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आज चर्चा में है। दरअसल गांधी के तीन रूप हैं। एक महात्मा गांधी दूसरा सत्याग्रही गांधी तीसरा हिंद स्वराज वाला गांधी। महात्मा गांधी और सत्याग्रही गांधी की की चर्चा पिछले शताब्दी में खूब हुई है। लेकिन इस समय जिस गांधी की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है वह है ‘ हिंद स्वराज’ वाला गांधी । इसलिए इस पुस्तक में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लेख हिन्द स्वराज पर है।
पिछले दो शताब्दियों के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि विश्व के जिन दो महापुरुषों ने दुनिया को अपने विचारों से सर्वाधिक प्रभावित किया वह है कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गांधी । कार्ल मार्क्स ने संकट की जड़ पूंजीवादी व्यवस्था में ढूंढा । उन्होंने न केवल पूंजीवादी व्यवस्था की समीक्षा की बल्कि उसके विकल्प के रूप में समाजवादी व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर चल कर दुनिया की एक बड़ी आबादी लगभग 70 सालों तक चलकर फिर वापस पूंजीवादी व्यवस्था के अंग बन गये । महात्मा गांधी कुछ अलग सोचते थे। उन्होंने संकट की जड़ आधुनिक औद्योगिक सभ्यता और उसके नियामक मूल्यों में तलाशा। इसलिए इस किताब में हिंद स्वराज के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की चर्चा विस्तार से की गई है और बहुत ही सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । बहुत सारे लोग मानते हैं कि गांधीजी मशीनों के खिलाफ थे। लेकिन स्वयं गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि उनका विरोध यंत्रों के लिए नहीं बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन है उसके लिए है। इस विषय पर बहुत ही गहराई से चर्चा इस किताब में की गई है ।
गांधी की सभ्यता -दर्शन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानते हैं कि हिंदुस्तान के पतन का मुख्य कारण उसका धर्म से च्युत होना है। लेकिन गांधी का आशय हिंदू ,मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म से नहीं है बल्कि धर्मों के अंदर जो धर्म है गांधी उसकी बात करते हैं । गांधी के लिए धर्म से च्युत होने का मतलब परमात्मा से अलग होना है । इसका बहुत ही सुंदर ढंग से विश्लेषण इस किताब में किया गया है। लेखक कहता है कि “जब सत्य समझ में आ जाता है तब धर्म का सही स्वरूप भी समझ में आ जाता है , क्योंकि तब यह भी समझ में आता है कि एक ही परम सत्य के अनंत अभिव्यक्तियों होने के कारण यहां सब अभिन्न है। कोई दूसरा नहीं है जिसका शोषण किया जा सकता जा सके। इसी समझ से लोक कल्याण के मूल्य नि:सृत होते हैं । गांधी इसी धर्म की बात करते हैं। इसलिए वे किसी धर्मनिरपेक्ष सभ्यता की वकालत नहीं करते, बल्कि धर्म सापेक्ष सभ्यता की स्वीकृति देते हैं। धर्म उनकी सभ्यता से बहिष्कृत नहीं है, बल्कि इसमें अनिवार्य रूप से स्वीकृत है।”
आधुनिक सभ्यता लोभ, भोग और ईष्या पर आधारित है । इसलिए गांधी ने इसे खारिज किया था, और प्रेम, सहयोग और सदुपयोग पर आधारित वैकल्पिक सभ्यता की बात की थी। इसके संपूर्ण आयाम पर बहुत ही विस्तार से इस लेख में प्रकाश डाला गया है ,जो इस पुस्तक को पठनीय के साथ संग्रहणीय बनाता है। लेखक के शब्दों में ‘ गांधी हिंद स्वराज में दया, परोपकार, प्रेम, सहिष्णुता आदि सद्गुणों वाले आदमी को केंद्र में रखकर सभ्यता संबंधी चिंतन प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनकी किताब और उनका चिंतन की आज भी उपादेयता है। इस सभ्यता को संकट से बचाने के लिए मानवीय मूल्य प्रदाता के रूप में गांधी आज भी प्रासंगिक है । इसलिए उनकी पुस्तक हिंद स्वराज और उसमें प्रतिपादित उनका सभ्यता दर्शन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। लेखक का यह भी मानना है कि विज्ञान के आतंक से मानव को मुक्त कर निर्भय समाज की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों के प्रणेता के रूप में गांधी की प्रासंगिकता आज भी है । यह बहुत कड़ा बयान है। महात्मा गांधी ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात की थी । उन्होंने माना कि बिना मानवीय दृष्टिकोण के विज्ञान दुनिया के सात महापाप में से एक है । (science without humanity is one of seven sins of world ). आचार्य विनोबा भावे ने इसका विस्तार किया । उन्होंने विज्ञान के सयानेपन की बात की । उन्होंने कहा विज्ञान और राजनीति का मेल विनाश है, तथा विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय सर्वोदय है। इसलिए विज्ञान के आतंक वाले बयान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
दूसरा महत्वपूर्ण लेख भूमंडलीकरण के युग में गांधी का सर्वोदय : औचित्य की तलाश भूमंडलीकरण एक भ्रामक शब्द है । इससे यह आभास होता है कि एकीकृत दुनिया में यह सर्वजन हिताय का उद्घोष है । मगर हकीकत में अमेरिका और पश्चिम के अमीर देशों के हित में विश्व बैंक , विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संरक्षण एवं निर्देशन में यह गरीब और विकासशील देशों के संसाधनों एवं बाजार पर कब्जा करने की मुहिम है । इसका वैचारिक पोषण उत्तर आधुनिकता के विचारों से मिलता है । इस विचारधारा के मूल में वह अनुभव है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित संचार युग और उपभोक्तावादी संस्कृति के समन्वय से पैदा हुआ है ।यह भूमंडलीकरण के प्रचार-प्रसार का विचारधारा है । इसका सविस्तार वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। लेखक का कहना है कि भूमंडलीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार की प्रक्रिया है । भूमंडलीकरण कुछ थोड़े से पूंजीवादी प्रतिष्ठानों द्वारा सारी दुनिया के गरीब, आम जनों के शोषण की व्यवस्था है । अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण कोई देश उनके क्रियाकलापों का खुलकर विरोध नहीं कर सकता इसलिए इसका खेल बेरोक -टोक जारी है।
इन सब कारणों से दुनिया भर में स्थानीय संघर्षों की बाढ़ आती है। वर्तमान केंद्रित राज्यों की शक्ति और हथियारों की क्षमता बहुत बढ़ गई है। उनके खिलाफ संघर्ष प्रायः आतंकवादी रूप ग्रहण करते हैं । इससे अराजक स्थितियॉ पैदा होती है । लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। हिंसक संघर्षों का सिलसिला अटूट बनता जाता है जिससे समाधान के बजाय सर्वनाश की संभावना बढ़ती है। दुनिया के गैर औद्योगिक देशों को आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में तब्दील करने की प्रक्रिया में संसार के संसाधनों का तेजी से दोहन होता है तथा औद्योगिक उत्सर्जन से पर्यावरण का संकट पैदा होता है। अमेरिका के रुख से स्पष्ट है कि अपनी समृद्धि को कायम रखने के लिए यह दुनिया को नष्ट होने का जोखिम उठाने को तैयार है । इस विनाश से बचने के लिए वैकल्पिक औद्योगिक ढांचे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत भी महसूस की जाने लगी है।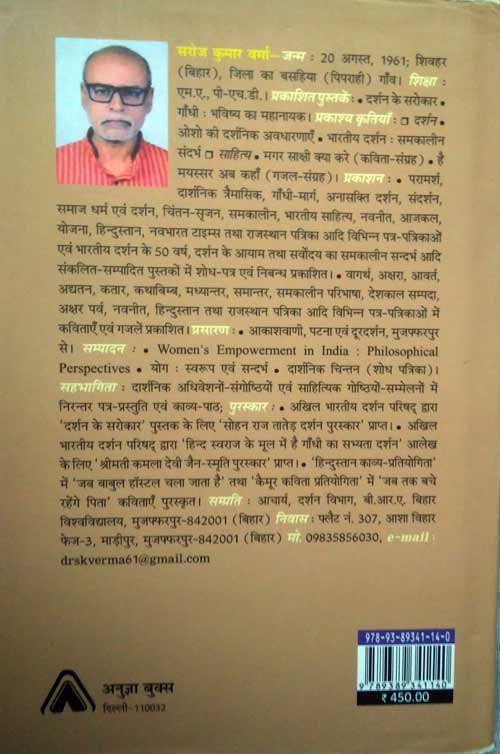
लेखक का मानना है कि भूमंडलीकरण से जो त्रासदियां पैदा हो रही है उनका शमन गांधी के सर्वोदय से हो सकता है। गांधी ने जिस तरह की जीवन पद्धति, समाज व्यवस्था, आर्थिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रिया आदि की हिमायत की जिससे शोषण का कोई तंत्र विकसित ही नहीं हो सके। इन सबका सम्मिलित रूप सर्वोदय है । अतः यह कहा जा सकता है कि सर्वोदय गांधी के तरकस में वह चीज है जिससे भूमंडलीकरण का चक्रव्यूह भेदा जा सकता है।
भूमंडलीकरण के इस युग में सर्वोदय की प्रासंगिकता और बढ़ गई है तथा वह और भी औचित्यपूर्ण हो गया है। भूमंडलीकरण और सर्वोदय दोनों के मूल्य अलग-अलग हैं। भूमंडलीकरण भौतिकवादी मूल्यों पर आधारित अवधारणा है, जबकि सर्वोदय आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित अवधारणा। इस अभिन्नता की वजह से भूमंडलीकरण केवल आर्थिक प्रयोजना बनकर रह गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सारी दुनिया को एक करना चाहता है , जबकि सर्वोदय सब के उदय के रूप में जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों का भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण करना है।
गांधी चिंतन में पर्यावरणीय चिंता आलेख में गांधी के पर्यावरणीय विचार को परखने की कवायद है । दरअसल लोभ और भोग पर आधारित पश्चिमी विकास के मॉडल के कारण आज दुनिया में पर्यावरण का संकट गहराता जा रहा है। इसका विस्तृत पड़ताल इस आलेख में है । हम विकास के उस रास्ते पर चल पड़े हैं इसमें नदियां सूख रही हैं और जमीन बंजर बन रहा है। जंगल समाप्त हो रहे है तथा पहाड़ खोदे जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है । संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन, जिसका नेतृत्व टिम लेंटन ने किया और इसमें चीन , अमेरिका और यूरोपियन देश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया, के अनुसार अगले 50 साल में धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है । जिससे दुनिया की तीन अरब गरीब आबादी प्रभावित होगी । इस तथाकथित विकास की बलिवेदी पर पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ गई है ।
महात्मा गांधी युग दृष्टा थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण सौ साल बाद होने वाली घटनाओं को साफ-साफ देख सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में ही विनाश के बीज निहित है। उन्होंने वर्तमान सभ्यता को अंतहीन इच्छाओं और शैतानियां के सोच से प्रेरित बताया था । आरोग्य की कुंजी पुस्तक में उन्होंने कहा इस शरीर को तीन प्रकार के प्राकृतिक पोषण की आवश्यकता है हवा , पानी और भोजन । उसमें हवा सबसे आवश्यक है। उन्होंने 1 जनवरी, 1918 को अहमदाबाद की एक बैठक में आजादी के तीन तत्व वायु ,जल और अनाज की आजादी के रूप में परिभाषित किया । उन्होंने जो तब कहा था वह सौ साल बाद अदालतें जीवन के अधिकार कानून की व्याख्या करते हुए साफ हवा , पानी और पर्याप्त भोजन के अधिकार के रूप में परिभाषित कर रही है। गांधी ने आज से लगभग आठ दशक पहले कहा था अगर भारत पश्चिम के विकास मॉडल का अनुसरण करेगा तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अलग धरती की आवश्यकता होगी।
गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य जब भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर के संसाधनों का उपभोग करेगा तो इससे प्रकृति की अर्थव्यवस्था नष्ट होगी। टाइम्स मैगजीन ने 9 अप्रैल उन्नीस सौ 2007 को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 51 सुझाव छापे थे उसमें 51 वां सुझाव कम उपभोग, ज्यादा साझेदारी और सरल जीवन बताया गया। यानी टाइम जैसी मैगजीन जिसे पश्चिम देशों का मुखपत्र कहा जाता है गांधी का रास्ता अपनाने के लिए कह रही है ।
लेखक का मानना है कि ‘ यद्यपि गांधी को तकनीकी अर्थ में दार्शनिक नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रुप से दर्शन की तत्वमीमांसीय अथवा ज्ञानमीमांसीय शब्दावली में अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, परन्तु उनमें सैकड़ों वर्ष पूर्व भविष्य को देख लेने की जो दूरदृष्टि थी वह उन्हें व्यवहारिक दार्शनिक के रुप में मजबूती से स्थापित कर देती है। यह स्थापना देश और दुनिया के लिए जितनी उपयोगी है , उतनी तकनीकी दार्शनिकों की स्थापनाएं नहीं। इसलिए समाज उसे सहजता से समझ लेता है और वे लोकप्रिय और प्रेरक सिद्ध होते हैं।
गांधी का सत्याग्रह : मानवाधिकारों के मात्रात्मक संरक्षक की प्रविधि आलेख में सत्याग्रह से मानव अधिकार की प्राप्ति एवं संरक्षण हो सकता है कि नहीं की पड़ताल की गई है । सत्याग्रह यानी सत्य के लिए अहिंसापूर्वक आग्रह। सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग है। लेखक का कहना है कि सत्याग्रह गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्य और अहिंसा पर आधारित स्वराज्य प्राप्ति की प्रविधि है । लेकिन स्वयं गांधीजी मानते थे की सत्याग्रह नित्य वस्तु है, जीवन की वस्तु है। सत्याग्रह जीवन की निष्ठा है । विनोबा के शब्दों में सत्याग्रह जीवन पद्धति , एक कार्य पद्धति और विशिष्ट प्रसंगों में उपाय पद्धति है। लेखक का यह भी कहना है कि गांधी के लिए सत्याग्रह विरोधियों से अपनी बात मनवाने का सर्वथा कारगर उपाय था। सत्याग्रह हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ यह समझना होगा कि अहिंसा एक अंत:शक्ति है। वह अनेक क्षेत्रों में काम करती है। थोड़ा व्यक्त करती है और बहुत सा अव्यक्त। हिंसा में बाहर की क्रिया ज्यादा होती है, अन्दर का सोचना क्षीण होता है। इसलिए चिंतन पर जब प्रहार होता है, तब हिंसा टिकती नहीं। इस वास्ते हिंसा का मुकाबला जब अहिंसा करेगी तो अव्यक्त रुप से करेगी। उसका मुख्य प्रहार सूक्ष्म में होगा। हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया उसका माध्यम होगा।
लेखक का मानना है कि स्वयं गांधीजी का देश विभाजन के मुद्दे पर सत्याग्रह नहीं करना और विभाजन के बाद दंगों का फैलना सत्याग्रह की सफलता को सीमित कर देता है। उनका यह भी मानना है कि उनके संगी साथियों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ । पहली बात तो यह कि जिस कालखंड की बात की जा रही है उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य की वस्तुपरख दृष्टिकोण के अभाव में अगर हम अतीत के सवाल को वर्तमान के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो सत्य तक पहुंचने के बजाय भ्रम में पहुंचने की संभावना ज्यादा है । इसलिए इतिहास के बारे में संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।
गांधीजी हमेशा कहा करते थे ” सत्याग्रह नित्य विकासशील शास्त्र है और आज तक हम इसका शास्त्र बना नहीं पाए।” गांधी जी ने नोआखाली और कोलकाता में जो सत्याग्रह किया वह उनके द्वारा किए गए सत्याग्रहों सर्वश्रेष्ठ था। जिसके बारे में तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने कहा था कि जो काम 50000 सैनिक नहीं कर पाए वह अकेले महात्मा गांधी ने कर दिया और उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दोनों सत्याग्रह सांप्रदायिक सौहार्द बहाली के लिए था। सत्याग्रही के लिए की चित्त निर्मलता परम आवश्यक है। इसके अभाव में सत्याग्रह दुराग्रह हो जाता है । कांग्रेस ने कभी भी अहिंसा और गांधी के रचनात्मक कार्य को हृदय से अंगीकार नहीं किया। अगर किया होता तो आज देश का इतिहास कुछ और होता। उन्होंने गांधीजी को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया।
गांधी जी ने राजनीति का अध्यात्मीकरण का जो प्रयास किया था वह सत्ता प्राप्ति की आहट के साथ ही धूमिल पड़ गया। अचार्य विनोबा भावे , जिन्हें गांधी ने 1940 में पहला सत्याग्रही घोषित किया था, का कहना है कि ‘ ज्यों ही सत्ता प्राप्ति के आसार दूर से दिखाई देने लगे त्यों ही राजनीति में अध्यात्मीकरण का जो आभा प्रकट हुआ था वह उड़ गया। आध्यात्मीकरण का बल दुर्बल पड़ गया । जहां पता चला कि सत्ता अब हाथ में आ रही है, वही राजनीति में अध्यात्म लगभग छोड़ दिया और गांधी जी से भी कह दिया गया कि अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं — पार्टिंग ऑफ वेज हो गया । कांग्रेस कमेटी ने गांधीजी को साफ-साफ सुना दिया कि अंग्रेज हमारी अमुक अमुक शर्तें स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें युद्ध में और अन्य सभी प्रकार की मदद देंगे। अहिंसा आदि के जो कुछ विचार हैं उन्हें छोड़ देंगे । यह कहकर उन्हें गांधी जी को अलग कर दिया।’ विनोबा कहते हैं कि “मुझे महाभारत की एक बात याद आ गई। जिस प्रकार दुर्योधन भगवान को छोड़ सेना लेकर खुश हुआ कि वह सेना के बल पर लड़ाई जीतेगा। उसी प्रकार इन लोगों ने गांधीजी को छोड़ सेना आदि लेना ठीक समझा
पुस्तक का दूसरा खंड तुलनात्मक अध्ययन का है । पहले आलेख में महावीर और गांधी की अहिंसा का तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारत में अहिंसा की परंपरा , महावीर और गांधी की अहिंसा में समानता और अंतर को स्पष्टता से रेखांकित किया गया है । लेकिन लेखक का यह मानना है कि गांधी तर्क के बिना दूसरों पर दबाव डालते थे, जो तथ्यों से परे है तथा इस पुस्तक के मूल स्थापना से मेल नहीं खाता। लेखक ने यह भी कहा है कि गांधी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे विरोधी विचारधारा के बारे में तल्ख टिप्पणी की है जो उनकी बौद्धिक अहिंसा को शिथिलता के प्रमाण है।
सवाल उठता है कि गांधी ने पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता की बड़ी तल्ख टिप्पणी की है , उसे शैतानी तक कहा है। जिस पर इस पुस्तक में भी विस्तार से चर्चा है । तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए इससे गांधी की अहिंसा खंडित – मंडित हो गई । इस तरह की कोई चर्चा इस पुस्तक में देखने को नहीं मिलती। यह विरोधाभासी स्थिति है। इससे बचा जा सकता था । दूसरी बात असहमत होना और विरोधी मानना दो अलग बातें हैं। गांधी ने कभी किसी को विरोधी नहीं माना जिनके अनगणित प्रमाण उनके जीवन में देखने को मिलता है। तीसरी बात कठोरता और कटुता में फर्क होता है और दोनों को मिला देने से चीजें गडमड हो जाती है। निश्चित रूप से लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से गांधी विचार को समझने परखने का प्रयास किया है ,जो सराहनीय कदम है। मगर गांधी की अहिंसा, सत्याग्रह पर और अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
पुस्तक में गांधी और विवेकानंद के सभ्यता विचार का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। गांधी ने जहां पश्चिम की सभ्यता को खारिज किया था और भारतीय सभ्यता को श्रेष्ट बताया था वही शुरुआत में विवेकानंद पश्चिम की चमक-दमक से काफी प्रभावित थे। बहुत बाद में उनका उससे मोहभंग होता है । लेकिन दोनों ने गरीबों , दरिद्रनारायण की सेवा की बात की। इन तमाम बिन्दुओं पर इस आलेख में विस्तार से वर्णन पढने को को मिलता है। जहाँ टैगोर का ईश्वर सौंदर्य और प्रेम रूप है वहां गांधी सत्य को ईश्वर मानते हैं। टैगोर और गांधी दोनों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनुभूति को आवश्यक मानते। इन सभी बिंदुओं पर टैगोर और गांधी के ईश्वर विचार में सविस्तार विश्लेषण पढ़ने को मिलता है।
इस पुस्तक में श्री अरविंद और गांधी के शिक्षण दर्शन पर भी प्रकाश डाला गया । श्री अरविंद जहां आत्म शिक्षण पर बल देते हैं वहां गांधी हृदय बुद्धि और शरीर तीनों के संतुलित विकास पर जोर देते है। श्री अरविंद के शिक्षा का मूल उद्देश्य आंतरिक आत्मिक विकास के साथ व्यक्ति को ऐसा बेहतर नागरिक बनाना है जो समाज के अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सके । गांधी का शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण करना मानते है उनका कहना था कि काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया अलग अलग नहीं हो सकती । जो शिक्षा हाथ पैर के इस्तेमाल के बिना दी जाएगी उसमें बुद्धि का सही विकास नहीं होगा और अगर होगा तो वह शैतान का घर होग। इस बात पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रकाश डाला गया है ।
हिंद स्वराज , सर्वोदय , सत्याग्रह , अहिंसा , शिक्षा ,सभ्यता , ईश्वर विचार आदि विषयों पर विमर्श के माध्यम से लेखक ने गांधी विचार को समझने एवं परखने का जो सार्थक और सामयिक प्रयास किया है वह स्वागत योग्य है । यह पुस्तक अलग-अलग काल खंडों में लिखे गए लेखों का संग्रह है । इसलिए इसमें तारतम्यता की कमी एवं पुनरावृति जगह जगह देखने को मिलती है ,जो खटकता है और पुस्तक की गंभीरता को कम करता है । पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रवाह पूर्ण है । गांधी विचार को दर्शनशास्त्र के मापदंड पर सरल तरीके से समझने समझाने का जो प्रयास किया गया है वह इस पुस्तक की विशेषता है। कुल मिलाकर यह पुस्तक गांधी विचार को जानने – समझने में उपयोगी है।
अशोक भारत




Recent Comments